Amir Khusro / अमीर ख़ुसरो (1253-1325 ईस्वी) चौदहवीं सदी के हिन्दी खड़ी बोली के पहले लोकप्रिय कवि थे, जिन्होंने कई ग़ज़ल, ख़याल, कव्वाली, रुबाई और तराना आदि की रचनाएँ की थीं। वे सूफीयाना कवि थे और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के मुरीद भी थे। इनका वास्तविक नाम था – अबुल हसन यमीनुद्दीन मुहम्मद। अमीर खुसरो दहलवी ने धार्मिक संकीर्णता और राजनीतिक छल कपट की उथल-पुथल से भरे माहौल में रहकर हिन्दू-मुस्लिम एवं राष्ट्रीय एकता, प्रेम, सौहादर्य, मानवतावाद और सांस्कृतिक समन्वय के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम किया। आइये जाने आमिर खुसरो का जीवन परिचय के बारे में (amir khusro ka jivan parichay in hindi)
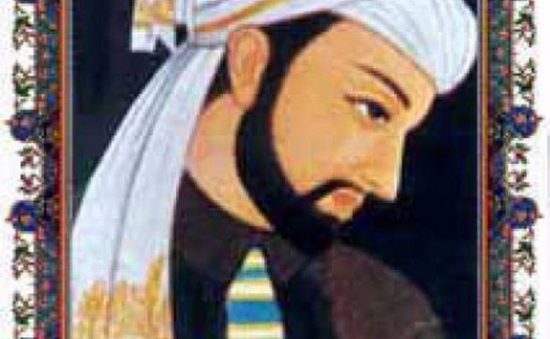
अमीर ख़ुसरो जीवन परिचय – Amir Khusro Biography in Hindi
| नाम | कवि अमीर खुसरो |
| जन्म | सन् 1235 |
| आयु | 70 वर्ष |
| जन्म स्थान | उत्तर प्रदेश |
| पिता का नाम | तुर्क सैफुद्दीन |
| माता का नाम | बलबनके |
| पत्नी का नाम | ज्ञात नहीं |
| बच्चे | ज्ञात नहीं |
| मृत्यु | अक्टूबर 1325 |
| मृत्यु स्थान | दिल्ली |
| प्रसिद्धि का कारण | कवि, संगीतकार |
प्रारंभिक जीवन – Early Life of Amir Khusrow
अमीर ख़ुसरो का जन्म सन 1253 ई. में एटा (उत्तरप्रदेश) के पटियाली नामक क़स्बे में गंगा किनारे हुआ था। इनके पिता ने इनका नाम ‘अबुल हसन’ रखा था। वे मध्य एशिया की लाचन जाति के तुर्क सैफ़ुद्दीन के पुत्र थे। लाचन जाति के तुर्क चंगेज़ ख़ाँ के आक्रमणों से पीड़ित होकर बलबन (1266-1286 ई.) के राज्यकाल में शरणार्थी के रूप में भारत आकर बसे थे।
हालाँकि अमीर ख़ुसरो का जन्म-स्थान काफ़ी विवादास्पद है। भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध यह है कि वे उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले के ‘पटियाली’ नाम के स्थान पर पैदा हुए थे। कुछ लोगों ने गलती से ‘पटियाली’ को ‘पटियाला’ भी कर दिया है, यद्यपि पटियाला से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था, हाँ, पटियाली से अवश्य था। पटियाली के दूसरे नाम मोमिनपुर तथा मोमिनाबाद भी मिलते हैं। पटियाली में इनके जन्म की बात हुमायूँ के काल के हामिद बिन फ़जलुल्लाह जमाली ने अपने ‘तज़किरा’ सैरुल आरफ़ीन’ में सबसे पहले कही। उसी के आधार पर बाद में लोग उनका जन्म पटियाली होने की बात लिखते और करते रहे। हिन्दी, उर्दू तथा अंग्रेजी की प्रायः सभी किताबों में उनका जन्म पटियाली में ही माना गया है। ए.जी.आर्बरी की प्रसिद्ध पुस्तक ‘क्लासिकल मर्शियन लिट्रेचर’ तथा ‘एनासाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका’ जैसे प्रामाणिक ग्रन्थों में भी यही मान्यता है।
ख़ुसरो की माँ एक ऐसे परिवार की थीं जो मूलतः हिन्दू था तथा इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। इनकी मातृभाषा हिंदी थी। इनके नाना का नाम रावल एमादुलमुल्क था। ये बाद में नवाब एमादुलमुल्क के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा बलबन के युद्धमंत्री बने। ये ही मुसलमान बने थे। इनके घर में सारे-रस्मो-रिवाज हिन्दुओं के थे। ये दिल्ली में ही रहते थे। कुछ लोगों के अनुसार ये कुल तीन भाई थे। सबसे बड़े इज़्ज़ुदीन आलीशाह जो अरबी-फ़ारसी के विद्वान थे, दूसरे हिसामुद्दीन जो अपने पिता की तरह योद्धा थे और तीसरे अबुल हसन जो कवि थे तथा आगे चलकर जो ‘अमीर ख़ुसरो’ नाम से प्रसिद्ध हुए।
अमीर खुसरो को बचपन से ही कविता करने का शौक़ था। ख़ुसरो के ननिहाल में गाने-बजाने और संगीत का माहौल था। ख़ुसरो के नाना को पान खाने का बेहद शौक़ था। इस पर बाद में ख़ुसरो ने ‘तम्बोला’ नामक एक मसनवी भी लिखी। इस मिले-जुले घराने एवं दो परम्पराओं के मेल का असर किशोर ख़ुसरो पर पड़ा। वे जीवन में कुछ अलग हट कर करना चाहते थे और वाक़ई ऐसा हुआ भी।
ख़ुसरो के श्याम वर्ण रईस नाना इमादुल्मुल्क और पिता अमीर सैफ़ुद्दीन दोनों ही चिश्तिया सूफ़ी सम्प्रदाय के महान् सूफ़ी साधक एवं संत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया उर्फ़ सुल्तानुल मशायख के भक्त अथवा मुरीद थे। उनके समस्त परिवार ने औलिया साहब से धर्मदीक्षा ली थी। उस समय ख़ुसरो केवल सात वर्ष के थे। सात वर्ष की अवस्था में ख़ुसरो के पिता का देहान्त हो गया, किन्तु ख़ुसरो की शिक्षा-दीक्षा में बाधा नहीं आयी।
अमीर ख़ुसरो आठ वर्ष की अवस्था से ही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य हो गये थे और सम्भवत: गुरु की प्रेरणा से ही उन्होंने काव्य-साधना प्रारम्भ की। यह गुरु का ही प्रभाव था कि राज-दरबार के वैभव के बीच रहते हुए भी ख़ुसरो हृदय से रहस्यवादी सूफी सन्त बन गये। ख़ुसरो ने अपने गुरु का मुक्त कंठ से यशोगान किया है और अपनी मसनवियों में उन्हें सम्राट से पहले स्मरण किया है।
अपने समय के दर्शन तथा विज्ञान में उन्होंने विद्वत्ता प्राप्त की, किन्तु उनकी प्रतिभा बाल्यावस्था में ही काव्योन्मुख थी। किशोरावस्था में उन्होंने कविता लिखना प्रारम्भ किया और 20 वर्ष के होते-होते वे कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गये।
जन्मजात कवि होते हुए भी ख़ुसरो में व्यावहारिक बुद्धि की कमी नहीं थी। सामाजिक जीवन की उन्होंने कभी अवहेलना नहीं की। जहाँ एक ओर उनमें एक कलाकार की उच्च कल्पनाशीलता थी, वहीं दूसरी ओर वे अपने समय के सामाजिक जीवन के उपयुक्त कूटनीतिक व्यवहार-कुशलता में भी दक्ष थे। उस समय बृद्धिजीवी कलाकारों के लिए आजीविका का सबसे उत्तम साधन राज्याश्रय ही था।
ख़ुसरो ने भी अपना सम्पूर्ण जीवन राज्याश्रय में बिताया। उन्होंने ग़ुलाम, ख़िलजी और तुग़लक़-तीन अफ़ग़ान राज-वंशों तथा 11 सुल्तानों का उत्थान-पतन अपनी आँखों से देखा। आश्चर्य यह है कि निरन्तर राजदरबार में रहने पर भी ख़ुसरो ने कभी भी उन राजनीतिक षड्यन्त्रों में किंचिन्मात्र भाग नहीं लिया जो प्रत्येक उत्तराधिकार के समय अनिवार्य रूप से होते थे। राजनीतिक दाँव-पेंच से अपने को सदैव अनासक्त रखते हुए ख़ुसरो निरन्तर एक कवि, कलाकार, संगीतज्ञ और सैनिक ही बने रहे। ख़ुसरो की व्यावहारिक बुद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि वे जिस आश्रयदाता के कृपापात्र और सम्मानभाजक रहे, उसके हत्यारे उत्तराधिकारी ने भी उन्हें उसी प्रकार आदर और सम्मान प्रदान किया।
साहित्या के अतिरिक्त संगीत के क्षेत्र में भी खुसरो का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने भारतीय और ईरानी रागों का सुन्दर मिश्रण किया और एक नवीन राग शैली इमान, जिल्फ़, साजगरी आदि को जन्म दिया। भारतीय गायन में क़व्वाली और सितार को इन्हीं की देन माना जाता है। इन्होंने गीत की तर्ज पर फ़ारसी में और अरबी ग़जल के शब्दों को मिलाकर कई पहेलियाँ और दोहे लिखे।
कहा जाता है कि तबला हज़ारों साल पुराना वाद्ययंत्र है किन्तु नवीनतम ऐतिहासिक वर्णन में बताया जाता है कि 13वीं शताब्दी में भारतीय कवि तथा संगीतज्ञ अमीर ख़ुसरो ने पखावज के दो टुकड़े करके तबले का आविष्कार किया।
ख़ुसरो की हिन्दी फारसी, तुर्की, अरबी तथा संस्कृत आदि कई भाषाओं में गति थी, साथ ही दर्शन, धर्मशास्त्र, इतिहास, युद्ध-विद्या व्याकरण, ज्योतिष संगीत आदि का भी उन्होंने अध्ययन किया था। इतने अधिक विषयों में ज्ञानार्जन का श्रेय ख़ुसरो कि विद्या-व्यसनी प्रकृति एवं प्रवृत्ति को तो है ही, साथ ही पिता की मृत्यु के बाद नाना एमादुलमुल्क के संरक्षण को भी है, जिनकी सभा में कवि, विद्वान एवं संगीतज्ञ आदि प्रायः आया करते थे, जिनमें ख़ुसरो को सहज ही सत्संग-लाभ का अवसर मिला करता था।
विवाह तथा सन्तान – Amir Khusrow Personal Life
ख़ुसरो के विवाह के सम्बन्ध में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु यह निश्चित है कि उनका विवाह हुआ था। उनकी पुस्तक ‘लैला मजनू’ से पता चलता है कि उनके एक पुत्री थी, जिसका तत्कालीन सामाजिक प्रवृत्ति के अनुसार उन्हें दुःख था। उन्होंने उक्त ग्रन्थ में अपनी पुत्री को सम्बोधित करके कहा है कि या तो तुम पैदा न होतीं या पैदा होतीं भी तो पुत्र रूप में। एक पुत्री के अतिरिक्त, उनके तीन पुत्र भी थे, जिनमें एक का नाम मलिक अहमद था। यह कवि था और सुल्तान फ़ीरोजशाह के दरबार से इसका सम्बन्ध था।
मृत्यु – Amir Khusrow Death
ख़ुसरो की अन्तिम ऐतिहासिक मसनवी ‘तुग़लक़’ नामक है जो उन्होंने ग़यासुद्दीन तुग़लक़ के राज्य-काल में लिखी और जिसे उन्होंने उसी सुल्तान को समर्पित किया। सुल्तान के साथ ख़ुसरो बंगाल के आक्रमण में भी सम्मिलित थे। उनकी अनुपस्थिति में ही दिल्ली में उनके गुरु शेख निज़ामुद्दीन मृत्यु हो गयी। इस शोक को अमीर ख़ुसरो सहन नहीं कर सके और दिल्ली लौटने पर 6 मास के भीतर ही सन 1325 ई. में ख़ुसरो ने भी अपनी इहलीला समाप्त कर दी। ख़ुसरो की समाधि शेख की समाधि के पास ही बनायी गयी।
देश-प्रेम
ख़ुसरो में देश-प्रेम कूट-कूट कर भरा था। उन्हें अपनी मात्रभूमि भारत पर गर्व था। ‘नुह सिपहर’ में भारतीय पक्षियों का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि यहाँ की मैना के समान अरब और ईरान में कोई पक्षी नहीं है। इसी प्रकार भारतीय मोर की भी उन्होंने बहुत प्रशंसा की है। उनकी रचनाओं में कई स्थानों पर भारतीय ज्ञान, दर्शन, अतिथि-सत्कार, फूलों-वृक्षों, रीति-रिवाजों तथा सौन्दर्य की मुक्तकंठ से प्रशंसा मिलती है। वे अपने को बड़े गर्व के साथ हिन्दुस्तानी तुर्क कहा करते थे।
अमीर खुसरो की लोकप्रिय अवधी कवितायें – Amir Khusro Poems in Hindi
दोहे
खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग
तन मेरो मन पियो को, दोउ भए एक रंग
खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वा की धार
जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार
खीर पकायी जतन से, चरखा दिया जला
आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा
गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस
चल खुसरो घर आपने, सांझ भयी चहु देस
खुसरो मौला के रुठते, पीर के सरने जाय
कहे खुसरो पीर के रुठते, मौला नहिं होत सहाय
उलटबांसियां
भार भुजावन हम गए, पल्ले बांधी ऊन
कुत्ता चरखा लै गयो, काएते फटकूंगी चून
काकी फूफा घर में हैं कि नायं, नायं तो नन्देऊ
पांवरो होय तो ला दे ला कथूरा में डोराई डारि लाऊं
खीर पकाई जतन से और चरखा दिया जलाय
आयो कुत्तो खा गयो तू बैठी ढोल बजाय, ला पानी पिलाय
भैंस चढ़ी बबूल पर और लपलप गूलर खाय
दुम उठा के देखा तो पूरनमासी के तीन दिन
पीपल पकी पपेलियां झड़ झड़ पड़े हैं बेर
सर में लगा खटाक से वाह रे तेरी मिठास.
लखु आवे लखु जावे, बड़ो कर धम्मकला
पीपर तन की न मानूं बरतन धधरया बड़ो कर धम्मकला
भैंस चढ़ी बबूल पर और लप लप गूलर खाए
उतर उतर परमेश्वरी तेरा मठा सिरानों जाए
भैंस चढ़ी बिटोरी और लप लप गूलर खाए
उतर आ मेरे सांड की, कहीं हिफ्ज न फट जाए.
FAQ
खुसरो किसका दरबारी था?
अमीर खुसरो (1253-1325) बलबन, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे।
अमीर खुसरो कौन था वह क्यों प्रसिद्ध हैं?
अमीर खुसरो एक इंडो-फ़ारसी सूफ़ी गायक, संगीतकार, कवि और विद्वान थे।
और अधिक लेख –
Please Note :- Amir Khusro Life History & Story In Hindi मे दी गयी Information अच्छी लगी हो तो कृपया हमारा फ़ेसबुक (Facebook) पेज लाइक करे या कोई टिप्पणी (Comments) हो तो नीचे करे।

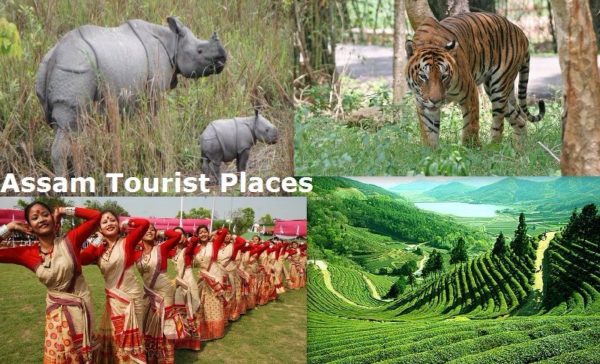
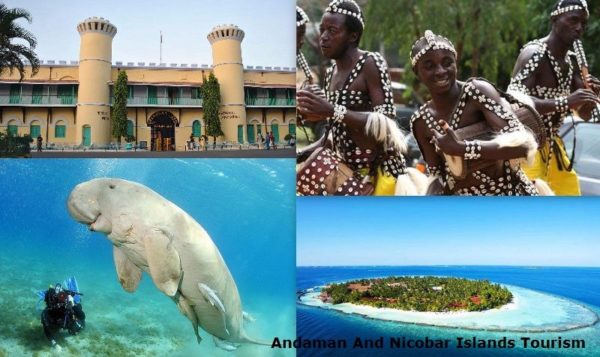
Amir khusro is the lagend great parsnaility.
AMIR KHUSRO JESA SHAYAR KOI NHI